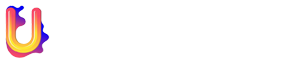रीवा रियासत
एक विस्तृत ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक प्रश्नोत्तरी
बघेल राजवंश, जिसे सोलंकी वंश की एक शाखा माना जाता है, ने बघेलखंड क्षेत्र पर सदियों तक शासन किया। उन्होंने दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य के उत्थान-पतन को देखा और कला, साहित्य व संगीत को उदारतापूर्वक संरक्षण दिया। नीचे दिए गए प्रश्नों के माध्यम से रीवा रियासत के गौरवशाली इतिहास और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बारे में अपने ज्ञान का परीक्षण करें।
ज्ञान परीक्षा: बघेल शासक
व्याघ्रदेव, गहोरा।
बघेल राजवंश के संस्थापक व्याघ्रदेव थे। उन्होंने 13वीं शताब्दी में उत्तर भारत की राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर गहोरा को अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाया और इस वंश की नींव डाली।
व्याघ्रदेव, जिनका संबंध गुजरात के वाघेला शासकों से था, ने 13वीं शताब्दी में सबसे पहले मारफा के किले पर विजय प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने गहोरा को अपनी राजधानी बनाकर एक नए राजवंश की स्थापना की, जिसे बाद में उन्हीं के वंश के नाम पर 'बघेलखंड' कहा गया।
रामचंद्र बघेल।
संगीत सम्राट मियां तानसेन, सम्राट अकबर के दरबार में जाने से पहले, रीवा के महाराजा रामचंद्र बघेल के दरबारी गायक थे। यहीं पर उनकी संगीत प्रतिभा को वास्तविक सम्मान और निखार मिला।
महाराजा रामचंद्र बघेल कला और संगीत के महान संरक्षक थे और उनका शासनकाल सांस्कृतिक दृष्टि से स्वर्ण युग माना जाता है। विश्व प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन प्रारंभ में इन्हीं के दरबार की शोभा थे। तानसेन की ख्याति सुनकर ही अकबर ने उन्हें अपने नवरत्नों में शामिल होने के लिए रीवा से आगरा बुलवाया था।
वीरभानु सिंह।
महाराजा वीरभानु सिंह ने चौसा के युद्ध (1539) में शेरशाह सूरी से पराजित होने के बाद मुगल सम्राट हुमायूँ को बांधवगढ़ के सुरक्षित किले में शरण दी थी।
यह एक अत्यंत साहसिक और उदारतापूर्ण कार्य था, क्योंकि ऐसा करके उन्होंने शक्तिशाली शेरशाह सूरी से सीधी शत्रुता मोल ले ली थी। इस घटना ने भविष्य के लिए बघेल-मुगल संबंधों की एक मजबूत और मैत्रीपूर्ण आधारशिला रखी, जिसका लाभ बाद के बघेल शासकों को मिला।
अनूप सिंह।
महाराजा अनूप सिंह ने लगभग 1654 ईस्वी में बघेल रियासत की राजधानी को अभेद्य माने जाने वाले बांधवगढ़ के पहाड़ी दुर्ग से रीवा में स्थानांतरित किया।
महाराजा अनूप सिंह, जो औरंगजेब के समकालीन और विश्वसनीय सामंत थे, ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया। रीवा, नदियों के संगम पर स्थित होने के कारण व्यापार, संचार और प्रशासन के लिए अधिक उपयुक्त था। इस स्थानांतरण के पीछे मुगल साम्राज्य का बढ़ता प्रभाव और मैदानी इलाकों में प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने की आवश्यकता भी एक प्रमुख कारण था।
1812-13, जय सिंह देव।
रीवा रियासत ने महाराजा जय सिंह देव के शासनकाल में वर्ष 1812 और 1813 में दो चरणों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए।
पिंडारियों और मराठों के निरंतर विनाशकारी आक्रमणों से उत्पन्न अराजकता और असुरक्षा से राज्य को बचाने के लिए यह निर्णायक कदम उठाया गया। यद्यपि इससे राज्य को बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा मिली, लेकिन इसने रियासत की बाह्य संप्रभुता को समाप्त कर दिया और औपनिवेशिक नियंत्रण का एक नया अध्याय शुरू किया।
मार्तंड सिंह।
रीवा के अंतिम शासक महाराजा मार्तंड सिंह जुदेव को "सफेद बाघ की भूमि" के रूप में पहचान दिलाने का श्रेय जाता है। उन्होंने ही 1951 में 'मोहन' नामक पहले जीवित सफेद बाघ शावक को पकड़ा था।
महाराजा मार्तंड सिंह को विश्व स्तर पर सफेद बाघों के प्रजनक के रूप में अद्वितीय ख्याति प्राप्त है। 27 मई 1951 को उन्होंने मोहन नामक एक सफेद बाघ शावक को पकड़ा, जिसे गोविंदगढ़ के महल में पाला गया। मोहन से ही दुनिया भर में पाले जाने वाले अधिकांश सफेद बाघों की वंश परंपरा शुरू हुई।
ज्ञान परीक्षा: पुरातात्त्विक स्थल
देउरकोठार।
देउरकोठार, रीवा जिले में स्थित, विंध्य क्षेत्र का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध पुरातात्विक स्थल है। यहाँ 40 से अधिक बौद्ध स्तूपों के भग्नावशेष और अशोककालीन ब्राह्मी शिलालेख पाए गए हैं।
यह स्थल इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि बघेलखंड क्षेत्र मौर्य साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था और सम्राट अशोक की धम्म नीति का यहाँ गहरा प्रभाव था। माना जाता है कि यह स्थल प्राचीन दक्षिणापथ व्यापार मार्ग पर स्थित एक प्रमुख बौद्ध केंद्र था, जो पाटलिपुत्र को उज्जैन से जोड़ता था।
गुप्तकालीन।
बांधवगढ़ किले में गुप्तकालीन (चौथी-पांचवीं शताब्दी ईस्वी) कला के अद्भुत प्रमाण मिले हैं, जिनमें चट्टानों को काटकर बनाई गई भगवान विष्णु की विशाल शेषशायी प्रतिमा (लगभग 35 फीट लंबी) प्रमुख है।
यह किला न केवल बघेलों की अभेद्य राजधानी रहा, बल्कि इसका इतिहास बहुत प्राचीन है। शेषशायी विष्णु प्रतिमा के अलावा यहाँ वराह और मत्स्य अवतार की मूर्तियाँ तथा ब्राह्मी लिपि में खुदे लेख वाली गुफाएँ भी हैं, जो इसके ऐतिहासिक महत्व को दर्शाती हैं।
कोल्डीहवा।
यद्यपि यह स्थल वर्तमान प्रयागराज जिले में है, परन्तु यह बघेलखंड की सांस्कृतिक इकाई का हिस्सा है। बेलन नदी घाटी में स्थित कोल्डीहवा से विश्व में धान या चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्यों में से एक (लगभग 6500 ई.पू.) मिला है।
यह खोज इस बात का प्रमाण है कि इस क्षेत्र के मानव ने बहुत पहले ही स्थायी कृषि जीवन अपना लिया था। यहाँ से प्राप्त हस्तनिर्मित मृद्भांड, पत्थर की कुल्हाड़ियाँ और गोलाकार झोपड़ियों के अवशेष एक विकसित ग्रामीण संस्कृति की ओर संकेत करते हैं।
कल्चुरी, शैव।
रीवा जिले में स्थित गुर्गी-महसांव, त्रिपुरी के कल्चुरी शासकों के काल में मत्तमयूर शैव संप्रदाय का एक विशाल और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त केंद्र था।
इस संप्रदाय के आचार्य अपनी विद्वत्ता और तांत्रिक साधनाओं के लिए प्रसिद्ध थे और उन्हें कल्चुरी शासकों से विशेष संरक्षण प्राप्त था। यहाँ से सैकड़ों मंदिरों के भग्नावशेष और उत्कृष्ट शैव प्रतिमाएँ मिली हैं, जो कल्चुरी मूर्तिकला की पराकाष्ठा को दर्शाती हैं।
ज्ञान परीक्षा: विदेशी शक्तियों से संबंध
जौनपुर सल्तनत।
14वीं और 15वीं शताब्दी में, बघेल राज्य को पूर्व में एक नई और शक्तिशाली पड़ोसी शक्ति, जौनपुर की शर्की सल्तनत, का सामना करना पड़ा। बघेल शासकों, विशेषकर भैरवदेव को, शर्की सुल्तानों के साथ निरंतर सीमा संघर्षों में उलझना पड़ा।
शर्की सुल्तान अत्यंत महत्वाकांक्षी थे और उन्होंने अपनी सल्तनत का विस्तार करने के लिए बघेलखंड पर नियंत्रण स्थापित करने के कई सैन्य अभियान चलाए। इस चुनौती से निपटने के लिए, बघेलों ने दिल्ली के लोधी सुल्तानों के साथ अवसरवादी गठबंधन बनाने का भी प्रयास किया।
मराठा और पिंडारी।
18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के पतन के बाद, रीवा रियासत को नागपुर के भोंसले मराठों और पिंडारियों के विनाशकारी आक्रमणों का सामना करना पड़ा। इन आक्रमणों ने रियासत की आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से चरमरा दिया।
मराठों ने चौथ और सरदेशमुखी की वसूली के लिए कई बार आक्रमण किए, जबकि पिंडारियों का एकमात्र लक्ष्य लूटपाट, विनाश और आतंक फैलाना था। इन आक्रमणों से उत्पन्न भयावह असुरक्षा ने ही रीवा को ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार करने पर विवश किया।
ब्रिटिश समर्थक।
1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महाराजा रघुराज सिंह ने अपनी संधि के प्रति निष्ठा दिखाते हुए ब्रिटिशों का सक्रिय रूप से समर्थन किया। उन्होंने ब्रिटिश सैनिकों को अपने राज्य में सुरक्षित आश्रय दिया और विद्रोह को कुचलने में मदद की।
उनकी इस वफादारी के पुरस्कार स्वरूप ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें 'नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया' (KCSI) की प्रतिष्ठित उपाधि से सम्मानित किया गया। हालांकि, यह एक विडंबना है कि उनके ही एक प्रमुख सरदार, ठाकुर रणमत सिंह, ने विद्रोहियों का साथ दिया और वीरतापूर्वक लड़े।
ज्ञान परीक्षा: साहित्य एवं स्रोत
वीरभानूदय काव्यम्।
'वीरभानूदय काव्यम्' एक संस्कृत महाकाव्य है जिसकी रचना कवि माधव ने 16वीं शताब्दी में महाराजा वीरभानु सिंह के संरक्षण में की थी। यह उनके जीवन, शासन और चरित्र का एक अमूल्य एवं प्रामाणिक स्रोत है।
यह ग्रंथ बघेल दृष्टिकोण को समझने में सहायक है और फारसी तवारीखों के पूरक के रूप में कार्य करता है। इसमें विशेष रूप से मुगल सम्राट हुमायूँ को शरण देने की ऐतिहासिक घटना का बहुत सुंदर और विस्तृत वर्णन किया गया है।
अकबरनामा।
अबुल फजल द्वारा रचित 'अकबरनामा' में महाराजा रामचंद्र बघेल, उनके वैभवशाली दरबार, और संगीत सम्राट तानसेन के अकबर के दरबार में आगमन की घटना का विस्तृत और प्रामाणिक वर्णन मिलता है।
यह ग्रंथ मुगल-बघेल संबंधों को समझने के लिए एक अनिवार्य स्रोत है। इसमें कालिंजर के किले को मुगलों को सौंपने की घटना का भी उल्लेख है। ये स्रोत मुख्य रूप से मुगल दृष्टिकोण से घटनाओं का वर्णन करते हैं, लेकिन बघेल शासकों की राजनीतिक स्थिति को समझने के लिए अमूल्य हैं।
आनंद रघुनंदन, विश्वनाथ सिंह।
कई प्रमुख विद्वान (जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल) 'आनंद रघुनंदन' नाटक को हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक होने का गौरव देते हैं। इसकी रचना महाराजा विश्वनाथ सिंह (1835-1854) ने की थी, जो स्वयं एक विद्वान और कवि थे।
रीवा दरबार हिंदी साहित्य के उत्थान का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। महाराजा विश्वनाथ सिंह और उनके पुत्र महाराजा रघुराज सिंह, दोनों ही कुशल कवि थे और उन्होंने कई भक्तिपूर्ण रचनाएँ कीं। इस प्रकार, रीवा दरबार ने हिंदी नाटक और कविता के प्रारंभिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
ज्ञान परीक्षा: सांस्कृतिक विरासत
सुंदरजा।
रीवा के गोविंदगढ़ का 'सुंदरजा आम' अपनी अनूठी सुगंध, स्वाद और बिना रेशे वाले गूदे के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसे अब भौगोलिक संकेतक (GI) टैग भी प्राप्त हो चुका है।
गोविंदगढ़, जो बघेल महाराजाओं की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, न केवल अपने किले और तालाब के लिए, बल्कि इन खास आम के बागों के लिए भी प्रसिद्ध है। यह आम बघेलखंड की कृषि विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसकी मांग देश-विदेश में है।
टी.आर.एस. कॉलेज।
ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय (टी.आर.एस. कॉलेज), जिसे पहले दरबार कॉलेज कहा जाता था, विंध्य क्षेत्र में उच्च शिक्षा का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित केंद्र है।
रीवा में आधुनिक शिक्षा की नींव महाराजा रघुराज सिंह ने रखी, लेकिन इसे संस्थागत रूप महाराजा व्यंकट रमण सिंह ने प्रदान किया। उन्होंने 1884 में दरबार कॉलेज की स्थापना की, जिससे शिक्षा का प्रसार आम लोगों तक हुआ और रियासत के आधुनिकीकरण की एक मजबूत नींव पड़ी।
बघेली।
बघेली, बघेलखंड क्षेत्र की प्रमुख लोकभाषा है, जो पूर्वी हिंदी की एक महत्वपूर्ण और मधुर बोली मानी जाती है। इसका लोक साहित्य अत्यंत समृद्ध है।
बघेली में लोकगीत (फाग, सोहर, बिरहा), लोककथाएँ और पहेलियाँ बहुतायत में मौजूद हैं, जो इस क्षेत्र की आत्मा और सांस्कृतिक पहचान को व्यक्त करती हैं। रीवा दरबार ने बघेली के साथ-साथ हिंदी और संस्कृत को भी निरंतर संरक्षण प्रदान किया।
महामृत्युंजय मंदिर।
रीवा के किले के भीतर स्थित महामृत्युंजय मंदिर भारत के कुछ विशिष्ट महामृत्युंजय ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है और यह बघेल राजपरिवार का कुलदेवता स्थल रहा है।
यह मंदिर आज भी रीवा और आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए आस्था का एक प्रमुख केंद्र है। कल्चुरी काल से ही इस क्षेत्र में शैव मत का गहरा प्रभाव रहा है और महामृत्युंजय मंदिर उसी परंपरा की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसे बघेल शासकों ने आगे बढ़ाया।
व्याघ्रदेव को परंपरागत रूप से बघेल (वाघेला) राजवंश का संस्थापक माना जाता है, जिनका मूल संबंध गुजरात के सोलंकी और वाघेला शासकों से था। वे गुजरात के वाघेला शासक वीर धवल के पुत्र थे और गुजरात से पूर्व की ओर आए थे। 13वीं शताब्दी के मध्य में, जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद उत्तर भारत में राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई थी और चंदेल तथा कल्चुरी जैसी क्षेत्रीय शक्तियाँ पतन की ओर थीं, व्याघ्रदेव ने इस राजनीतिक शून्य का लाभ उठाया। उन्होंने अपनी सैन्य प्रतिभा और दूरदर्शिता का परिचय देते हुए सबसे पहले कालिंजर के दक्षिण-पूर्व में स्थित मारफा (वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बाँदा जिले में) के अभेद्य किले पर अधिकार स्थापित किया। यह उनकी पहली महत्वपूर्ण विजय थी जिसने इस क्षेत्र में उनके आगमन की घोषणा की। इसके पश्चात, उन्होंने गहोरा (चित्रकूट के निकट, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित) को अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाया और यहीं से बघेल शासन की नींव डाली। उनका यह कदम अत्यंत रणनीतिक था, क्योंकि यह स्थान दिल्ली और पूर्व की शक्तियों के बीच एक बफर जोन में स्थित था। व्याघ्रदेव ने न केवल एक नए राजवंश की स्थापना की, बल्कि उन्होंने इस क्षेत्र को एक नई राजनीतिक पहचान भी दी, जिसे बाद में उन्हीं के वंश के नाम पर 'बघेलखण्ड' कहा गया।
महाराजा रामचंद्र बघेल का शासनकाल बघेल राजवंश के इतिहास में सांस्कृतिक दृष्टि से स्वर्ण युग माना जाता है। वे मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे और उनके साथ उनके घनिष्ठ एवं मैत्रीपूर्ण संबंध थे, जिसकी नींव उनके पिता वीरभानु ने हुमायूँ की मदद करके रखी थी। महाराजा रामचंद्र कला, साहित्य और संगीत के महान संरक्षक और पारखी थे। विश्व प्रसिद्ध संगीत सम्राट मियां तानसेन प्रारंभ में इन्हीं के दरबारी गायक थे और यहीं उनके संगीत को वास्तविक सम्मान और निखार मिला। तानसेन की ख्याति सुनकर ही अकबर ने अपने दरबारी जलाल खान कोरची को भेजकर उन्हें अपने नवरत्नों में शामिल करने के लिए रीवा से आगरा बुलवाया था। कहा जाता है कि बीरबल भी कुछ समय तक महाराजा रामचंद्र के दरबार से जुड़े रहे थे। राजनीतिक रूप से, उन्होंने 1569 में, कालिंजर का किला अकबर को सौंपकर मुगलों से एक औपचारिक संधि की और उनकी अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन इसके बदले में उन्होंने अपने राज्य में पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता बनाए रखी। उनका दरबार उस समय उत्तर भारत के सबसे प्रतिष्ठित सांस्कृतिक केंद्रों में से एक था।
महाराजा वीरभानु सिंह का शासनकाल बघेल इतिहास में उनके शौर्य, उदारता और कूटनीतिक कौशल के लिए विख्यात है। उनके दरबारी कवि माधव द्वारा रचित संस्कृत महाकाव्य 'वीरभानूदय काव्यम्' उनके जीवन, शासन और चरित्र का एक अमूल्य एवं प्रामाणिक स्रोत है। वे मुगल सम्राट हुमायूँ और सूर वंश के शेरशाह सूरी के समकालीन थे। उनके शासनकाल की सबसे उल्लेखनीय और दूरगामी परिणाम वाली ऐतिहासिक घटना चौसा के युद्ध (1539) में शेरशाह सूरी से बुरी तरह पराजित होने के बाद, असहाय और भागे हुए मुगल सम्राट हुमायूँ को बांधवगढ़ के सुरक्षित किले में शरण देना और उनकी हरसंभव सहायता करना था। यह एक अत्यंत साहसिक और उदारतापूर्ण कार्य था, क्योंकि ऐसा करके उन्होंने शक्तिशाली शेरशाह सूरी से सीधी शत्रुता मोल ले ली थी। इस घटना ने भविष्य के लिए बघेल-मुगल संबंधों की एक मजबूत और मैत्रीपूर्ण आधारशिला रखी, जिसका लाभ बाद के बघेल शासकों को मिला। वीरभानु ने शेरशाह सूरी के आक्रमणों का भी सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया और कठिन परिस्थितियों में भी अपने राज्य की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखा।
महाराजा अनूप सिंह का शासनकाल बघेल इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। वे मुगल सम्राट शाहजहाँ और औरंगजेब के समकालीन थे। वे औरंगजेब के विश्वसनीय सामंतों में गिने जाते थे और उन्होंने मुगल साम्राज्य के दक्षिण अभियानों, विशेषकर गोलकुंडा और बीजापुर के विरुद्ध अभियानों में महत्वपूर्ण सैन्य भूमिका निभाई थी। उनकी वफादारी और सेवाओं से प्रसन्न होकर औरंगजेब ने उन्हें 'महाराजा' की उपाधि प्रदान की थी। उनका सबसे महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रभाव वाला कार्य लगभग 1654 ईस्वी के आसपास राजधानी को सामरिक दृष्टि से अत्यंत सुरक्षित माने जाने वाले बांधवगढ़ के पहाड़ी दुर्ग से रीवा में स्थानांतरित करना था। रीवा, टोंस और बीहर नदियों के संगम के निकट स्थित होने के कारण व्यापार, संचार और प्रशासनिक दृष्टि से अधिक उपयुक्त था। इस स्थानांतरण के पीछे मुगल साम्राज्य का बढ़ता प्रभाव और मैदानी इलाकों में प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने की आवश्यकता भी एक प्रमुख कारण हो सकती है। उन्होंने रीवा शहर की विधिवत नींव रखी, किले का निर्माण करवाया और इसके प्रारंभिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे रीवा बघेलखंड का नया राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र बन गया।
महाराजा जय सिंह देव का शासनकाल रीवा के इतिहास में एक युगांतकारी मोड़ था। उन्होंने अपने पूर्ववर्ती शासकों के समय हुए पिंडारियों और मराठों के निरंतर विनाशकारी आक्रमणों से उत्पन्न अराजकता, आर्थिक विनाश और राजनीतिक असुरक्षा का दंश झेला था। राज्य को इस विनाश से बचाने और एक स्थायी शांति स्थापित करने के लिए, उन्होंने एक निर्णायक और दूरगामी कदम उठाया। वर्ष 1812 और 1813 में, उन्होंने दो चरणों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक सहायक संधि (Treaty of Subsidiary Alliance) पर हस्ताक्षर किए। इस संधि के माध्यम से रीवा रियासत औपचारिक रूप से ब्रिटिश संरक्षण में आ गई। इसके बदले में, अंग्रेजों ने रीवा को बाहरी आक्रमणों, विशेषकर पिंडारियों के आतंक से, सुरक्षा प्रदान करने का वचन दिया। यद्यपि इस संधि ने राज्य को तत्काल सुरक्षा और शांति प्रदान की, लेकिन इसने रियासत की बाह्य संप्रभुता को समाप्त कर दिया और रीवा के आंतरिक मामलों में ब्रिटिश रेजीडेंट के माध्यम से हस्तक्षेप का मार्ग प्रशस्त किया। यहीं से रीवा पर औपनिवेशिक नियंत्रण का एक नया अध्याय शुरू हुआ जो 1947 तक चला।
महाराजा मार्तंड सिंह जुदेव बघेल राजवंश के अंतिम शासक थे, जिन्होंने भारत के इतिहास के एक अत्यंत महत्वपूर्ण संक्रमण काल में शासन किया। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात, सरदार वल्लभभाई पटेल के नेतृत्व में चल रही रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया के तहत, उन्होंने 1948 में रीवा रियासत का भारतीय संघ में विलय करने के 'विलय पत्र' (Instrument of Accession) पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद रीवा, बघेलखंड की अन्य रियासतों के साथ मिलकर, नवगठित 'विंध्य प्रदेश' का हिस्सा बना। महाराजा मार्तंड सिंह को विंध्य प्रदेश (1948-1956) का प्रथम राजप्रमुख भी नियुक्त किया गया। बाद में वे भारतीय राजनीति में भी सक्रिय रहे और कई बार रीवा से लोकसभा के सदस्य (सांसद) चुने गए। महाराजा मार्तंड सिंह को विश्व स्तर पर सफेद बाघों के प्रजनक के रूप में अद्वितीय ख्याति प्राप्त है। 27 मई 1951 को उन्होंने मोहन नामक एक सफेद बाघ शावक को पकड़ा था, जिसे गोविंदगढ़ के महल में पाला गया। मोहन से ही दुनिया भर में पाले जाने वाले अधिकांश सफेद बाघों की वंश परंपरा शुरू हुई। उन्होंने रीवा को 'लैंड ऑफ व्हाइट टाइगर्स' के रूप में अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई।
देउरकोठार, रीवा जिले में स्थित, विंध्य क्षेत्र का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध पुरातात्विक स्थल है। यह स्थल इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि बघेलखंड क्षेत्र मौर्य साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था और सम्राट अशोक की धम्म नीति का यहाँ गहरा प्रभाव था। यहाँ लगभग 40 से अधिक विभिन्न आकार के बौद्ध स्तूपों के भग्नावशेष पाए गए हैं, जिनमें से कुछ ईंटों से बने विशाल स्तूप हैं। सबसे महत्वपूर्ण खोजों में अशोककालीन ब्राह्मी लिपि में लिखे गए तीन प्रस्तर स्तंभ लेख शामिल हैं। इन लेखों में सम्राट अशोक की धम्म नीति के सिद्धांतों और बौद्ध संघ के आचार्यों तथा अनुयायियों का स्पष्ट उल्लेख है। इसके अतिरिक्त, यहाँ से उत्तरी कृष्ण मार्जित मृद्भांड (NBPW), आहत सिक्के (Punch-marked coins), और टेराकोटा की वस्तुएँ भी प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुई हैं। माना जाता है कि यह स्थल प्राचीन दक्षिणापथ व्यापार मार्ग पर स्थित एक प्रमुख बौद्ध केंद्र और प्रशासनिक इकाई था, जो पाटलिपुत्र को कौशाम्बी, भरहुत और उज्जैन जैसे महत्वपूर्ण नगरों से जोड़ता था। यह स्थल मौर्यकालीन स्थापत्य और अभियांत्रिकी का भी उत्कृष्ट उदाहरण है।
बंधवगढ़ का किला एक अत्यंत प्राचीन, ऐतिहासिक और रणनीतिक महत्व का दुर्ग है, जो आज एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान के केंद्र में स्थित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, इसका निर्माण भगवान राम ने लंका से लौटने के बाद अपने भाई लक्ष्मण को भेंट करने के लिए करवाया था, इसीलिए इसका नाम 'बंधव-गढ़' (भाई का किला) पड़ा। पुरातात्विक दृष्टि से, यहाँ गुप्तकालीन (चौथी-पांचवीं शताब्दी ईस्वी) कला के अद्भुत प्रमाण मिले हैं, जिनमें चट्टानों को काटकर बनाई गई भगवान विष्णु की शेषशायी प्रतिमा (लगभग 35 फीट लंबी), तथा उनके वराह और मत्स्य अवतार की विशाल मूर्तियाँ प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त, यहाँ अनेक मानव निर्मित गुफाएँ हैं जिन पर ब्राह्मी लिपि में लेख खुदे हैं। यह किला लंबे समय तक, लगभग 1654 ई. तक, बघेल राजवंश की सबसे महत्वपूर्ण और अभेद्य राजधानी रहा। इसकी अभेद्यता की ख्याति पूरे भारत में थी। किले के भीतर कल्चुरी काल के अनेक मंदिरों के भग्नावशेष, प्राचीन जलस्रोत (तालाब), और आवासीय संरचनाओं के अवशेष आज भी इसके गौरवशाली और निरंतर आबाद रहने वाले अतीत की कहानी कहते हैं।
यद्यपि ये पुरातात्विक स्थल वर्तमान में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित हैं, परंतु बघेलखंड की सीमा के निकट होने और विंध्य क्षेत्र की समान सांस्कृतिक इकाई का हिस्सा होने के कारण इनका उल्लेख अत्यंत महत्वपूर्ण है। बेलन नदी घाटी में स्थित इन स्थलों ने भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाणिक क्रांति को समझने में अभूतपूर्व योगदान दिया है। कोल्डीहवा से विश्व में धान या चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्यों में से एक (लगभग 6500 ई.पू.) मिला है। यह खोज इस बात का प्रमाण है कि इस क्षेत्र के मानव ने बहुत पहले ही स्थायी कृषि जीवन अपना लिया था। इसके अतिरिक्त, यहाँ से रस्सी की छाप वाले हस्तनिर्मित और चाक-निर्मित मृद्भांड, पॉलिशदार पत्थर की कुल्हाड़ियाँ, हड्डी के उपकरण, और गोलाकार झोपड़ियों के अवशेष मिले हैं, जो एक विकसित ग्रामीण संस्कृति की ओर संकेत करते हैं। इसके निकट स्थित महगड़ा से एक विशाल पशु-बाड़े के साक्ष्य मिले हैं, जो बड़े पैमाने पर पशुपालन को इंगित करते हैं। ये स्थल मानव के शिकारी-संग्राहक जीवन से स्थायी कृषक जीवन में परिवर्तन के महत्वपूर्ण प्रमाण हैं।
रीवा जिले में स्थित गुर्गी और निकटवर्ती महसांव, त्रिपुरी के कल्चुरी शासकों के काल में मत्तमयूर शैव संप्रदाय का एक विशाल और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त केंद्र था। इस संप्रदाय के आचार्य अपनी गहन विद्वत्ता, तांत्रिक साधनाओं और दार्शनिक ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे और कल्चुरी शासकों से उन्हें विशेष संरक्षण प्राप्त था। कल्चुरी शासक युवराजदेव प्रथम ने मत्तमयूर आचार्य प्रभावशिव को यहाँ आमंत्रित कर एक विशाल मठ और मंदिर का निर्माण करवाया था। पुरातात्विक अन्वेषणों और उत्खनन में यहाँ से सैकड़ों मंदिरों, मठों, और विशाल तालाबों के भग्नावशेष मिले हैं। सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यहाँ से प्राप्त विशाल और कलात्मक दृष्टि से उत्कृष्ट शैव प्रतिमाएँ हैं, जिनमें नटराज, उमा-महेश्वर, कल्याणसुंदर (शिव-पार्वती विवाह), और विभिन्न देवी-देवताओं की मूर्तियाँ प्रमुख हैं। ये प्रतिमाएँ कल्चुरी मूर्तिकला की पराकाष्ठा को दर्शाती हैं। गुर्गी से प्राप्त अधिकांश मूर्तियाँ अब रीवा के वेंकट संग्रहालय और प्रयागराज संग्रहालय में प्रदर्शित हैं, जो इस स्थल के गौरवशाली अतीत की मूक गवाह हैं।
14वीं और 15वीं शताब्दी में, जब दिल्ली सल्तनत कमजोर पड़ी, तो बघेल राज्य को पूर्व में एक नई और शक्तिशाली पड़ोसी शक्ति, जौनपुर की शर्की सल्तनत, का सामना करना पड़ा। शर्की सुल्तान अत्यंत महत्वाकांक्षी थे और उन्होंने 'अटाला मस्जिद' जैसी भव्य इमारतों का निर्माण करवाया। उन्होंने अपनी सल्तनत का विस्तार करने के लिए बघेलखंड क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करने के कई सैन्य अभियान चलाए। बघेल शासकों, विशेषकर भैरवदेव (भैदचन्द्र), को शर्की सुल्तानों के साथ निरंतर सीमा संघर्षों में उलझना पड़ा। यह प्रतिद्वंद्विता बघेलों के लिए एक बड़ी चुनौती थी। इस चुनौती से निपटने के लिए, बघेलों ने एक चतुर कूटनीतिक चाल चली। उन्होंने जौनपुर के पश्चिमी प्रतिद्वंद्वी, दिल्ली के लोधी सुल्तानों, के साथ अवसरवादी गठबंधन बनाने के प्रयास किए, ताकि जौनपुर के दबाव को संतुलित किया जा सके। यह काल बघेलों के लिए दोहरी चुनौती का था, जिसमें उन्हें दो शक्तिशाली सल्तनतों के बीच अपनी स्वायत्तता और अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कुशल कूटनीति और सैन्य तैयारी का प्रदर्शन करना पड़ा।
मराठा और पिंडारी: आतंक का काल
18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर मराठा शक्ति का तेजी से उदय हुआ, जो बघेलखंड के लिए एक विनाशकारी काल साबित हुआ। विशेष रूप से नागपुर के भोंसले शासकों ने बघेलखंड पर चौथ और सरदेशमुखी की वसूली के लिए कई बार विनाशकारी आक्रमण किए। इन आक्रमणों से रियासत को भारी आर्थिक क्षति हुई, फसलें नष्ट कर दी गईं, और आम जनता को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसी काल में, मध्य भारत पिंडारियों के अनियंत्रित आतंक से भी त्रस्त था। पिंडारी मूल रूप से अनियमित घुड़सवार लड़ाके थे जिनका एकमात्र लक्ष्य केवल लूटपाट करना था। अमीर खान और चीतू पिंडारी जैसे सरदारों के नेतृत्व में पिंडारियों के दलों ने बघेलखंड क्षेत्र में कई बार भयानक और अमानवीय आक्रमण किए। इन आक्रमणों ने रीवा रियासत में पूरी तरह से कानून-व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया और एक भयावह असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया। मराठों और पिंडारियों के इसी आतंक ने अंततः रीवा के शासक, महाराजा जय सिंह देव, को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से सुरक्षा की गुहार लगाने और उनके साथ सहायक संधि करने के लिए अंतिम रूप से विवश कर दिया।
महाराजा रघुराज सिंह का लंबा शासनकाल रीवा रियासत के आधुनिकीकरण और प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने अपनी संधि के प्रति निष्ठा दिखाते हुए ब्रिटिशों का सक्रिय रूप से समर्थन किया। उन्होंने न केवल ब्रिटिश सैनिकों को अपने राज्य में सुरक्षित आश्रय दिया बल्कि विद्रोह को कुचलने में भी मदद की। उनकी इस वफादारी के पुरस्कार स्वरूप ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें 'नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया' (KCSI) की प्रतिष्ठित उपाधि से सम्मानित किया गया। हालांकि, यह विडंबना ही है कि उनके राज्य के एक प्रमुख सरदार, ठाकुर रणमत सिंह, ने विद्रोहियों का साथ दिया और ब्रिटिशों के विरुद्ध वीरतापूर्वक लड़े। रघुराज सिंह ने रियासत में कई प्रशासनिक सुधारों को गति दी। उन्होंने न्याय व्यवस्था में सुधार किए, सड़कों, स्कूलों और अस्पतालों का निर्माण करवाया। रीवा में पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना का श्रेय भी उन्हें ही जाता है। गोविंदगढ़ किले और उसके सुरम्य तालाब का निर्माण भी उनके समय की एक महत्वपूर्ण देन है, जो उनकी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी।
बघेल वंशावली एवं काव्य: स्थानीय स्वर
बघेल शासकों के संरक्षण में रचित वंशावलियाँ और काव्य ग्रंथ उनके वंश, शौर्य, और सांस्कृतिक योगदानों पर प्रकाश डालते हैं। ये ग्रंथ बघेल दृष्टिकोण को समझने में सहायक हैं और फारसी तवारीखों के पूरक के रूप में कार्य करते हैं। इनमें प्रमुख हैं: वीरभानूदय काव्यम्, जिसकी रचना कवि माधव ने 16वीं शताब्दी में महाराजा वीरभानु सिंह के संरक्षण में संस्कृत में की थी, और इसमें हुमायूँ को शरण देने की घटना का सुंदर वर्णन है। आनंद रघुनंदन नाटक, जिसकी रचना महाराजा विश्वनाथ सिंह (1835-1854) ने की, को कई विद्वान हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक होने का गौरव देते हैं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न कवियों द्वारा समय-समय पर रचित बघेल वंश वर्णनम् जैसी कृतियाँ हैं, जो शासकों की पीढ़ियों, उनकी उपलब्धियों और वंशावली का लेखा-जोखा प्रस्तुत करती हैं। ये ग्रंथ स्थानीय दृष्टिकोण, सांस्कृतिक मूल्यों, भाषा के विकास और परंपराओं को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और अनिवार्य स्रोत हैं।
मुगल दरबार में शाही संरक्षण में लिखे गए समकालीन फ़ारसी इतिवृत्त या तवारीख, बघेलखंड के इतिहास, विशेषकर मुगल-बघेल संबंधों, के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा में महाराजा रामचंद्र बघेल, उनके वैभवशाली दरबार, संगीत सम्राट तानसेन के अकबर के दरबार में आगमन, और कालिंजर के किले को मुगलों को सौंपने की घटना का विस्तृत और प्रामाणिक वर्णन मिलता है। इसी प्रकार, अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा रचित बादशाहनामा (शाहजहाँ के काल का इतिहास) में बघेल शासकों की मुगल अभियानों, विशेषकर दक्षिण के अभियानों में, भागीदारी और उनकी मनसबदारी का उल्लेख है। ये स्रोत मुख्य रूप से मुगल साम्राज्य के दृष्टिकोण से घटनाओं का वर्णन करते हैं, लेकिन बघेल शासकों की राजनीतिक स्थिति, मुगल दरबार के साथ उनके जटिल संबंधों और उस काल के सांस्कृतिक आदान-प्रदान को समझने के लिए ये अनिवार्य और अमूल्य स्रोत हैं।
बघेली व्यंजन: सादगी और स्वाद
बघेलखंड का पारंपरिक खान-पान यहाँ की कृषि और जलवायु के अनुरूप, सादगीपूर्ण, पौष्टिक और स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री पर आधारित है। यह स्वाद में अद्वितीय होता है। यहाँ के कुछ विशेष व्यंजन हैं:
- इंद्रहर: यह अरबी (घुइयां) के पत्तों और विभिन्न दालों (चना, उड़द, मूंग) के पिसे हुए मिश्रण से बनी एक प्रकार की स्वास्थ्यवर्धक बड़ियाँ होती हैं, जिन्हें पहले भाप में पकाया जाता है और फिर तेल में तलकर या रसेदार सब्जी के रूप में खाया जाता है।
- रिकमच: यह भी अरबी के पत्तों (रिकमच के पत्ता) को बेसन और मसालों के घोल के साथ परत-दर-परत लगाकर, रोल करके भाप में पकाया जाता है और फिर टुकड़ों में काटकर तला जाता है। यह एक लोकप्रिय नाश्ता है।
- दाल-बाटी: यद्यपि यह मूलतः राजस्थानी व्यंजन है, पर बघेलखंड में भी इसका खूब प्रचलन है और इसे स्थानीय स्वाद के अनुसार बनाया जाता है।
- स्थानीय अनाज: ज्वार, कोदो, कुटकी जैसे मोटे अनाजों का पारंपरिक भोजन में महत्वपूर्ण स्थान रहा है।
- सुंदरजा आम: रीवा के गोविंदगढ़ का सुंदरजा आम अपनी अनूठी सुगंध, स्वाद और बिना रेशे के गूदे के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसे अब जीआई टैग भी प्राप्त है।
रीवा रियासत में शिक्षा और विद्वता को संरक्षण देने की एक लंबी और गौरवशाली परंपरा रही है।
पारंपरिक शिक्षा: बघेल दरबारों में संस्कृत के विद्वानों, कवियों और ज्योतिषियों को सदैव आश्रय और उच्च सम्मान मिला। महाराजा रामचंद्र, विश्वनाथ सिंह, और रघुराज सिंह जैसे कई शासक स्वयं विद्वान और कवि थे। राज्य में कई स्थानों पर पारंपरिक संस्कृत पाठशालाएँ थीं, जहाँ छात्रों को व्याकरण, साहित्य, दर्शन और ज्योतिष की गहन शिक्षा दी जाती थी।
आधुनिक शिक्षा: रीवा में आधुनिक शिक्षा की नींव महाराजा रघुराज सिंह ने रखी, लेकिन इसे वास्तविक गति और संस्थागत रूप महाराजा व्यंकट रमण सिंह (1880-1918) ने प्रदान किया। उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझते हुए 1884 में दरबार कॉलेज की स्थापना की, जो आज ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय (टी.आर.एस. कॉलेज) के नाम से विख्यात है। यह इस संपूर्ण विंध्य क्षेत्र में उच्च शिक्षा का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित केंद्र है। उन्होंने रियासत में कई स्कूलों की भी स्थापना की, जिससे शिक्षा का प्रसार आम लोगों तक हुआ और रियासत के आधुनिकीकरण की एक मजबूत नींव पड़ी।
भाषा और साहित्य: बघेलखंड की आत्मा
बघेली: बघेलखंड क्षेत्र की यह प्रमुख लोकभाषा, पूर्वी हिंदी की एक महत्वपूर्ण और मधुर बोली है। बघेली में अत्यंत समृद्ध लोक साहित्य (लोकगीत, लोककथाएँ, पहेलियाँ) मौजूद है, जो इस क्षेत्र की आत्मा को व्यक्त करता है।
हिंदी का विकास: रीवा दरबार हिंदी साहित्य के उत्थान का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। महाराजा विश्वनाथ सिंह (1835-1854), जो स्वयं एक विद्वान और कवि थे, ने 'आनंद रघुनंदन' नामक नाटक की रचना की। इस कृति को कई प्रमुख विद्वान (जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल) हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक मानते हैं। उनके पुत्र, महाराजा रघुराज सिंह भी एक कुशल कवि थे और उन्होंने कई भक्तिपूर्ण रचनाएँ कीं। इस प्रकार, रीवा दरबार ने हिंदी नाटक और कविता के प्रारंभिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
संस्कृत: बघेल शासकों ने संस्कृत भाषा को भी निरंतर संरक्षण प्रदान किया। 'वीरभानूदय काव्यम्' और कल्चुरी काल के अनेक अभिलेख संस्कृत में ही हैं, जो इस भाषा की गहरी जड़ों को दर्शाते हैं।
टोंस (तमसा) और बीहर नदियों के संगम पर स्थित रीवा का किला बघेल राजवंश की शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक रहा, विशेषकर जब महाराजा अनूप सिंह ने 17वीं शताब्दी में राजधानी को बांधवगढ़ से यहाँ स्थानांतरित किया। यह किला केवल एक सैन्य दुर्ग ही नहीं, बल्कि एक विशाल प्रशासनिक और आवासीय परिसर भी था। किले के परिसर में कई महत्वपूर्ण संरचनाएँ हैं, जिनमें शाही महल (जिसके कुछ हिस्से आज भी राजपरिवार के निवास में हैं), रानी तालाब महल, और दरबार हॉल शामिल हैं। किले की वास्तुकला समय के साथ विकसित हुई और इसमें बघेल शैली के साथ-साथ मुगल और बाद में यूरोपीय (इंडो-सारासेनिक) प्रभाव भी स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। किले के भीतर स्थित महामृत्युंजय मंदिर भारत के कुछ विशिष्ट महामृत्युंजय ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है और यह बघेल राजपरिवार का कुलदेवता स्थल रहा है। यह मंदिर आज भी रीवा और आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए आस्था का एक प्रमुख केंद्र है। किला शहर के केंद्र में स्थित है और रीवा के इतिहास का एक जीवंत स्मारक है।